रामचरितमानस, रामचरितमानस चौपाई, रामचरितमानस चौपाई अर्थ सहित, रामचरितमानस, रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर pdf download, रामचरितमानस की चौपाई
Ramcharitmanas kya hai: “रामचरितमानस” गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधि भाषा में 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना संवत 1631 ई. की रामनवमी को अयोध्या में प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। उन्होंने इसे संवत 1633 [1576 ई.] में मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष में रामविवाह के दिन पूर्ण किया था।
इसका कुछ अंश काशी में भी निर्मित हुआ था। यह इसके किष्किन्धा कांड के प्रारंभ में आने वाले एक सोरठे से निकलती है। उसमे काशी का वर्णन मिलता है। इसके मुख्य छंद चौपाई और दोहा हैं। बीच-बीच में कुछ अन्य प्रकार के भी छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रायः 8 या अधिक अर्दलियों के बाद दोहा होता है। और इन दोहों के साथ कड़वक संख्या दी गयी है। इस प्रकार के समस्त कड़वकों की संख्या 1074 है।
इसे सामान्यतः ”तुलसी रामायण” या “तुलसीकृत रामायण” भी कहा जाता है। ‘रामचरितमानस” का भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व है। “रामचरितमानस” की प्रसिद्धि अद्वितीय है। उत्तर भारत में बहुत से लोगों द्वारा रामायण के रूप में इसे प्रतिदिन पढ़ा जाता है।
शरद नवरात्रि में इसके “सुन्दरकाण्ड” का पाठ पुरे 9 दिन किया जाता है। मंगलवार एवं शनिवार को इसके “सुन्दरकाण्ड” का पाठ किया जाता है। “रामचरितमानस” के नायक राम हैं। जिनको एक ”मर्यादा पुरषोत्तम” के रूप में दर्शाया गया है। जो की अखिल ब्रम्हांड के स्वामी “हरी नारायण” भगवान के अवतार हैं।
जबकि महर्षि बाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक आदर्श चरित्र मानव के रूप में दर्शाया गया है। जो सम्पूर्ण मानव समाज को ये सिखाता है कि, जीवन को किस प्रकार जिया जाये भले ही उसमे कितने ही विध्न हों। तुलसी के राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी ”मर्यादा पुरषोत्तम” हैं।
गोस्वामी जी ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों,चौपाइयों, सोरठी तथा छेद का आश्रय लेकर वर्णन किया है। रामचरितमानस को गोस्वामी जी ने 7 काण्डों [ अध्यायों] के नाम इस प्रकार हैं —-
- बालकांड
- अयोध्याकांड
- अरण्यकांड
- किष्किन्धा कांड
- सुन्दर कांड
- लंकाकांड [युद्धकांड]
- उत्तरकांड
छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किन्धा कांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी के अलंकारों का बहुत सुन्दर प्रयोग किया है। विशेषकर अनुप्रास अलंकार को “रामचरितमानस” में प्रत्येक हिन्दू की अनन्य आस्था है। और इसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है।
“रामचरितमानस” कथा का संक्षिप्त वर्णन
महाबलशाली एवं महाज्ञानी राक्षसराज रावण दक्षों से लंका जीतकर वहां राज्य करने लगा। पृथ्वी उसके अनाचारों एवं अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं के शरण में गयीं। इन सब ने मिलकर भगवान हरि से प्रार्थना की जिसके उत्तर में आकाशवाणी हुई कि, भगवान् हरि, दशरथ-कौशल्या के पुत्र के रूप में अयोध्या में अवतार लेंगे और समस्त राक्षसों का विनाश कर भूमि-भार हरण करेंगे ।
दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इस आश्वासन के अनुसार चैत्र के शुक्लपक्ष की नवमी को हरि ने कौशल्या के पुत्र के रूप में अवतार लिया। कौशल्या के गर्भ से ही एवं भगवान् हरि के शेषनाग ने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। जबकि कैकेयी ने भरत एवं सुमित्रा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया।
राम-लक्ष्मण ने राक्षसों से ऋषि मुनि को बचाया
इस समय राक्षसों का अत्याचार उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी प्रारंभ हो गया था। जिसके कारण ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। क्योकिं यज्ञ में राक्षस लोग बाधा उत्पन्न करते थे। जब ऋषि मुनि विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि, पृथ्वी पर भगवान् ”हरि” दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं।
तो वे अयोध्या आये और उस वक़्त राम बालक ही थे, तो उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए दशरथ से राम-लक्ष्मण की याचना की। राम तथा लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने अपना यज्ञपूर्ण किया। इन विध्नकारी राक्षसों में से एक सुबादु जो मारा गया और दूसरा मारीच था जो राम के बाणों से आहत होकर 100 योजन की दूरी पर समुद्र के पार चला गया।

राम सीता का विवाह
राम-लक्ष्मण जिस समय विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे, मिथिला में सीता के विवाह हेतु स्वयंवर आयोजित किया गया था। जिसके लिए ऋषि मुनि विश्वामित्र को आमंत्रित किया गया था। अतः ऋषि विश्वामित्र अपने साथ राम -लक्ष्मण को लेकर मिथिला गये।
मिथिला के राजा जनक ने देश-विदेश के समस्त राजाओं को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु आमंत्रित किया था। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राक्षस भी इस निमंत्रण पर वहां उपस्थित हुए थे। किन्तु स्वयंवर की शर्तों के अनुसार ,स्वयंवर में रखे हुए धनुष को तोड़ने वाले का ही विवाह सीता के साथ होगा। स्वयंवर में आमंत्रित समस्त राजाओं ने इसे तोड़ने का प्रयास किया परन्तु तोडना तो दूर वह सब इसे हिला भी नहीं पाए।
ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर राम ने सरलता से इस धनुष को तोड़ दिया। और सीता का वरण किया, जिसके पश्चात राजा जनक ने सीता से राम के विवाह के अवसर पर अयोध्या निमंत्रण भेजा। राजा दशरथ अपने शेष पुत्रों के साथ बारात लेकर मिथिला पहुंचे, एवं विवाह के पश्चात अपने चारों पुत्रों के साथ अयोध्या वापस आ गये।
कैकेयी की मांग पर राम को वनवास
दशरथ ने अपनी ढलती अवस्था पर राम को अपना युवराज पद देना चाहा। संयोगवश उस समय कैकेयी के पुत्र भरत एवं सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गये थे। कैकेयी की दासी मंथरा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने कैकेयी को भी यह बातें बतायीं।
पहले तो कैकेयी ने यह कहकर उसका अनुमोदन किया कि, पिता के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। यह उनके राजकुल की परंपरा है। किन्तु मंथरा के यह समझाने पर कि, भरत की अनुपस्थिति में यह जो आयोजन किया जा रहा है, उसमे कई दुरभि- संधि है, कैकेयी ने इस आयोजन को विफल बनाने का संकल्प किया, एवं कोप भवन में चली गयीं ।
तब उन्होंने दशरथ से उनके 2 वचन देने के रूप में एक से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरा भरत के लिए युवराज पद मांग लिया। इनमे से प्रथम वचन के अनुसार, जब राम ने वन के लिए प्रस्थान किया, तो सीता एवं लक्ष्मण भी वन के लिए उनके साथ चल दिए।
कुछ दिनों के पश्चात जब दशरथ ने राम के वियोग में शारीर त्याग दिया, तब भरत ननिहाल से बुलाये गये। और उन्हें अयोध्या का राज-पाठ सौंपा गया। किन्तु भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया, और वे राम को वापस लाने हेतु चित्रकूट जा पहुंचे। जहाँ उस समय राम निवास कर रहे थे। किन्तु राम ने लौटना स्वीकार नहीं किया।
भरत के अनुरोध पर उन्होंने अपनी चरण-पादुकाएं उन्हें दे दीं। जिन्हें अयोध्या लाकर भरत ने सिंहासन पर रख दिया। और वे राज कार्य देखने लगे। चित्रकूट से चल कर राम दक्षिण के जंगलों की और बढ़े। जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे। तब रावण की बहन शूर्पणखा एक मनमोहक रूप धारण कर वहां आयी, और राम के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा
राम के अस्वीकार करने पर उसने अपना वास्तविक भयंकर रूप प्रकट किया। यह देखकर राम के संकेत पर लक्ष्मण ने उसके नाक काट लिए। इस प्रकार कुरूप की हुई शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गयी और उन्हें राम से युद्ध करने हेतु प्रेरित किया।
खर-दूषण ने अपनी सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया। किन्तु वे अपनी समस्त सेना के साथ युद्ध में मारे गये। तब शूर्पणखा रावण के पास गयी, और सारा वृतांत सुनाया। रावण ने मारीच की मदद से, जिसे विश्वामित्र के आश्रम में राम ने युद्ध में आहत किया था। सीता का हरण किया, जिसके परिणाम स्वरुप राम को रावण से युद्ध करना पड़ा।
राम और रावण का युद्ध
इस परिस्थिति में राम ने किष्किन्धा के वानरों की सहायता ली और रावण पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ रावण का भाई विभीषण भी आकर राम के साथ हो गया। राम ने अंगद नाम के वानर को रावण के पास दूत के रूप में आखिरी बार सावधान करने हेतु भेजा कि, वह सीता को आदर-सम्मान के साथ वापस कर दें।
किन्तु रावण ने अपने अभिमान के बल पर इसे अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप राम तथा रावण के दलों में युद्ध छिड़ गया। अब महायुद्ध में रावण तथा उसके बंधू-बांधव मारे गये। इसके पश्चात लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप कर सीता को साथ लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आये। राम का राज्यभिषेक किया गया और दीर्घकाल तक उन्होंने प्रजरंजन करते हुए शासन किया ।
“रामचरितमानस” में छंदों की संख्या
“रामचरितमानस” में विविध छंदों की चौपाई – 9388, दोहा-1172, सोरठा -87, श्लोक -47, छंद-208, कुल-10902 [ चौपाई, दोहा, सोरठा ,श्लोक, छंद ] है।
नीति एवं सदाचार
“रामचरितमानस” भले राम कथा हो, किन्तु यह राम चरित्र के द्वारा नैतिकता एवं सदाचार की शिक्षा दे रहा है। “रामचरितमानस” भारतीय संस्कृति का वाहक महाकाव्य ही नही अपितु विश्वजनिन आचारशास्त्र का बोधक महान ग्रंथ भी है। यह धर्म के सिद्धांतों के प्रयोगात्मक पक्ष का आदर्श रोप प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है।
यह विभिन्न पूरण निगभागम सम्मत, लोकशास्त्र कव्यावेक्षणजन्य स्वानुभूति पुष्ट प्रातिभ चाक्षुष विषयीकृत जागतिक एवं पारमार्थिक तत्वों का सम्यक निरूपण करता है ।
गोस्वामी जी ने बताया है कि
नाना पुराण निगमागम सम्मत यद्रामायणे निग्दितन क्व्चिद्न्योडपि
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति।।
अर्थात यह ग्रंथ नाना पुराण, निगमागम, रामायण तथा कुछ अन्य ग्रंथों से लेकर रचा गया है। और तुलसी ने अपने अन्तः सुख के लिए रघुनाथ की गाथा कही है।
प्रसिद्ध ग्रंथ
अध्यात्म रामायण में राम ने इस प्रयोग में कहा है , ”माता मुझे भोजन करने का समय नही है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दण्डकरण्या जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया। वहां मुनि वेश में 14 वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, आप किसी प्रकार की चिंता न करें”।
मातृ वचन सुनी अति अनुकूला। जणू स्नेह सुरुतरू के फूला।।
सुख मकरंद भरेश्रिय मूला। निरखि राम मन भंवरु न भूला।।
धरम धुरीन धरम गाणी जानी। कहेउ मातृ सन अमृत वानी।।
पिता दीन्ह मोहि कानन राजू। जहाँ सब भांति भोर बड काजू।।
आयुस देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता।।
जनि स्नेह बस डरपति मोरे। आबहूँ अम्ब अनुग्रह तोरे।।
व्यवहारिकता
तुलसीदास इस अध्यात्मवाद की दुहाई न देकर अपने आदर्शवाद को अव्यवहारिक होने से बचा लेते हैं। वे राम को एक धर्म-निष्ठ नायक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जो पिता की आज्ञा का पालन करना अपना एक परम पुनीत कर्तव्य समझता है। इसलिए उन्होंने बताया कि,
धरम धुरीन धरम गतिजानी।
कहेऊ मातुसन अति मृदु बानी।
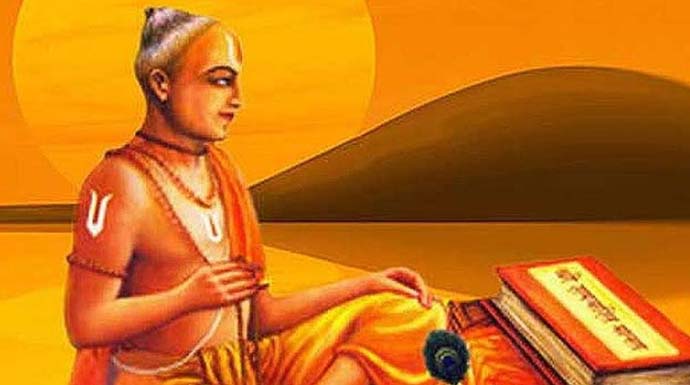
“रामचरितमानस” की लोकप्रियता
तुलसीदास की भक्ति की अभिव्यक्ति भी इसमें अत्यंतविषद रूप में हुई है। अपने अराध्य भगवान राम के सम्बन्ध में उन्होंने रामचरितमानस में अनेकों बार बताया है कि, “रामचरितमानस” में राम का चरित्र ही ऐसा है जो एक बार सुन लेता है, वह अनायास उनका भक्त हो जाता है।
वास्तव में तुलसीदास ने अपने अराध्य के चरित्र की इसी प्रकार की कल्पना भी की है। यही कारण है कि, इसने समस्त उत्तरी भारत पर सदियों से प्रभाव डाल रखा है। और यहाँ के अध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया है। घर-घर में ”रामचरितमानस” का पाठ पिछले साढ़े तीन शताब्दियों से होता आ रहा है।
और इसे एक धर्म ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसके आधार पर गाँव-गाँव में प्रतिवर्ष रामलीलाओं का आयोजन भी किया जाता है। उत्तरी भारत का यह सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। एवं जिस समय तक मानव जाती आदर्शों और जीवन के मूल्यों पर विश्वास रखेगी, “रामचरितमानस” को सम्मानपूर्वक स्मरण किया जाता रहेगा। यह कहने के लिए कदाचित भविष्यत-वक्ता की जरूरत नहीं है।
